विशेषाधिकार के हिलते ही उजागर होता पाखंड
UGC के नए रेगुलेशन आते ही सार्वजनिक विमर्श में जो दृश्य उभरा है, वह चौंकाने वाला जरूर है, पर अप्रत्याशित नहीं। वर्षों से जिन नारों, प्रतीकों और वैचारिक दावों को राष्ट्रवाद का पर्याय बताया जाता रहा, वे एक झटके में गायब हो गए। जो कल तक हिंदू राष्ट्र को हर बहस का केंद्र बनाते थे, वे आज इस्लाम से “गलबहियां” करने की सीख दे रहे हैं। जो वामपंथ को कोसना अपना धर्म समझते थे, वही अब वामपंथी होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। उग्र राष्ट्रवाद के स्वयंभू रक्षक अलग देश की मांग तक का उपदेश देने लगे हैं। और जिनके लिए कल तक प्रधानमंत्री अवतार थे, आज उन्हीं के खिलाफ ऐसी भाषा और प्रतीकात्मक हिंसा दिखाई दे रही है, जिसे लिखना भी शिष्टाचार के विरुद्ध है।
यह कोई अचानक आया नैतिक संकट नहीं है। यह उस प्रिविलेज का पर्दाफाश है, जो अब तक सुरक्षित था और आज खतरे में दिख रहा है। विशेषाधिकार हिलते ही वैचारिक पाखंड बेनकाब हो जाता है—इतिहास बार-बार यही सिखाता है।
भारत का इतिहास भी यही बताता है कि कुछ अपवादों—जैसे विदेशी आक्रांताओं के दौर—को छोड़ दें, तो यह देश आधुनिक अर्थों में राष्ट्र-राज्य की चेतना के साथ विकसित नहीं हुआ। राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया आज भी अधूरी है। इस अधूरेपन की सबसे बड़ी वजह है—जाति।
जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि एक बंद व्यवस्था है—जहाँ जन्म ही भाग्य तय करता है। वर्ग हर समाज में होते हैं, वर्गीय भेदभाव भी होता है, पर भारत की त्रासदी यह है कि यहाँ भेदभाव जन्म से स्थायी बना दिया गया। यही वजह है कि जाति भारत की एकता और बंधुत्व को सदियों से छलनी करती रही है—रिश्तों में, शादियों में, अवसरों में और सम्मान में।
विडंबना यह है कि जैसे ही जाति-उच्छेद की बात उठती है, उसे संस्कृति की आत्मा, समाज की रीढ़ और पहचान का आधार बताकर बचाने के लिए कुतर्कों की पूरी फौज खड़ी हो जाती है। यह रक्षा-कवच उसी अदृश्य लेकिन प्रभावशाली प्रिविलेज का है, जो आज असहज है—और इसलिए छटपटाहट है।
सच यह भी है कि जिस दिन जातियाँ समाप्त होंगी, उसी दिन जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट और भेदभाव-निरोधी रेगुलेशन अपने आप अप्रासंगिक हो जाएंगे। कोई भी समाज स्थायी रूप से बैसाखियों के सहारे नहीं चलता। ये उपाय रोग नहीं, रोग के लक्षण हैं। लेकिन लक्षणों पर बहस करना आसान है, रोग का इलाज कठिन।
दुखद यह है कि जाति-उच्छेद के लिए न कभी गंभीर कानूनी पहल हुई, न ही ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई दी। चरणबद्ध उच्छेद की बात तो दूर, उल्टा जाति को सामाजिक रूप से छुपाया गया और राजनीतिक रूप से संगठित किया गया। चुनावों में यह वोट बैंक बनती है और समाज में “संवेदनशील विषय” घोषित कर दी जाती है—ताकि असली सवाल कभी पूछा ही न जाए।
जब तक जाति पर यह सामूहिक चुप्पी और सुविधाजनक राजनीति जारी रहेगी, तब तक राष्ट्रवाद, विकास और समता—सब केवल नारे बने रहेंगे। UGC रेगुलेशन पर उठा शोर हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं—नारों के राष्ट्र की, या समान नागरिकों के राष्ट्र की।
निर्णय हमारे सामने है। विशेषाधिकार बचाने की राजनीति चुननी है, या न्यायपूर्ण समाज बनाने का साहस। इतिहास गवाह है—राष्ट्र वही बनते हैं, जो कठिन सवालों से भागते नहीं, उनका सामना करते हैं।
विशेषाधिकार के हिलते ही उजागर होता पाखंड
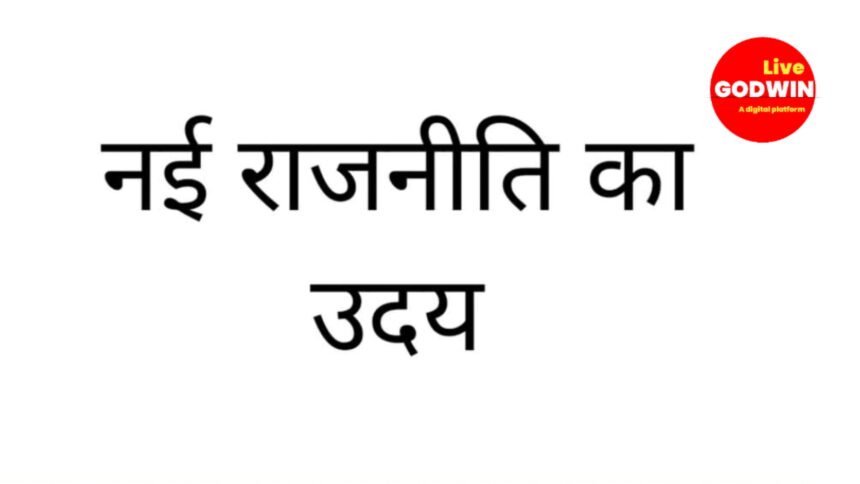
Leave a Comment Leave a Comment






